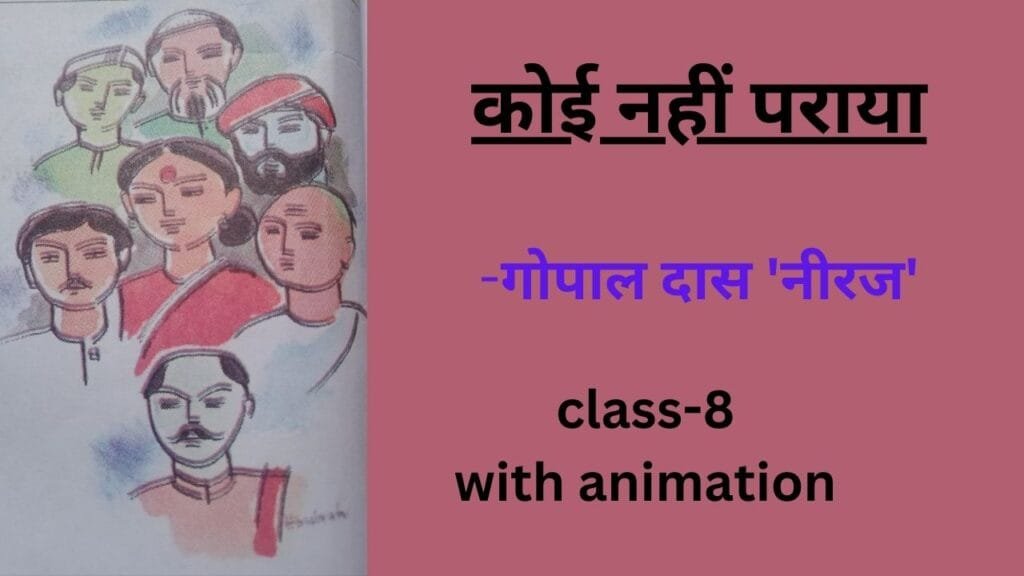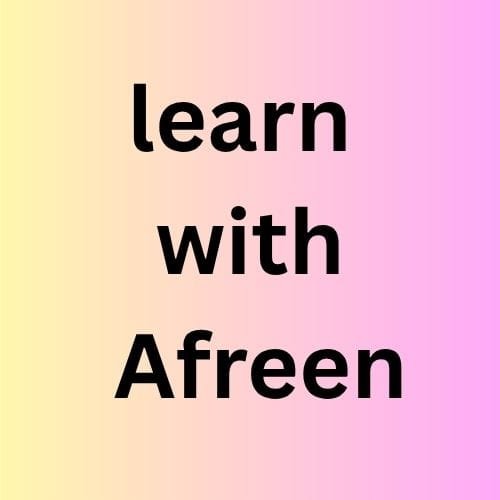Table of Contents
Toggleकोई नहीं पराया
-गोपाल दास 'नीरज'
संदर्भ:
यह काव्य पंक्तियाँ मानवता, प्रेम, और समस्त विश्व को एक परिवार मानने की भावना को व्यक्त करती हैं।
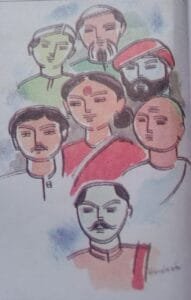 प्रसंग:
प्रसंग:
कवि ने इस कविता में इंसानियत, प्रेम और समता की बात की है। उन्होंने खुद को देश, काल, जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर बताया है। उनका मानना है कि सत्य धर्म वही है, जो सभी से प्रेम करना सिखाए। वह बाहरी प्रतीकों और मंदिर-मस्जिद की उपासना को अनावश्यक मानते हुए, मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं।
व्याख्या:
कवि कहते हैं कि उनके लिए कोई भी पराया नहीं है, उनका घर यह पूरा संसार है। वे न तो देश-काल की सीमाओं से बंधे हैं और न ही जाति-पाँति के संकीर्ण विचारों से। उनके लिए धर्म का अर्थ सिर्फ किताबों के शब्द नहीं है, बल्कि प्रेम है।
उनके विचार से ईश्वर का निवास हर व्यक्ति के हृदय में है, और इसलिए वे बाहरी पूजा स्थलों की आवश्यकता महसूस नहीं करते। उनके अनुसार, हर इंसान का हृदय ही देवालय है, जहाँ ईश्वर की उपासना की जा सकती है।
इस कविता में कवि मानवता के प्रति प्रेम, समर्पण और सहिष्णुता का भाव दर्शाते हैं।
संदर्भ:
इस कविता में कवि ने मानवता के प्रति अपने प्रेम और गर्व को व्यक्त किया है। कवि के अनुसार, इंसान के लिए प्रेम और मानवीय गुण ही सबसे अधिक महत्व रखते हैं।
प्रसंग:
कवि इस कविता में अपने मनुष्य होने पर गर्व व्यक्त करते हैं। वे मानवता को देवत्व और अमरत्व से श्रेष्ठ मानते हैं। कवि को धरती का प्रेम स्वर्ग के सुखों से भी अधिक प्यारा है। वे पूरी मानव जाति को एक परिवार के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं।
व्याख्या:
कवि कहते हैं कि चाहे इंसान कहीं भी रहे और किसी भी परिस्थिति में हो, उन्हें हर इंसान प्यारा है। वे अपनी मानवता पर गर्व करते हैं और देवत्व या ईश्वरत्व के बजाय मनुष्यत्व को ही अधिक प्रिय मानते हैं। कवि यह भी कहते हैं कि वे अमरत्व जैसे किसी अन्य लाभ को त्याग सकते हैं, लेकिन प्रेम को नहीं।
कवि को स्वर्ग की सुखद कहानियाँ सुनने में रुचि नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी धरती उन्हें सौ-सौ स्वर्गों से भी ज्यादा सुंदर लगती है। उनका दृष्टिकोण समग्र मानवता और अपने परिवेश के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता है।
इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि वे समस्त पृथ्वी को अपने घर की तरह मानते हैं, जहाँ सभी लोग उनके अपने हैं। उनके लिए मानवता और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और वे मानवता को ही सबसे महान धर्म मानते हैं।
(3)मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बाँट सको तुम बाँटो अपने प्यार को। हँसो इस तरह, हँसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाय पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल, जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे, पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है।
संदर्भ:
इस कविता में कवि ने जीने और दूसरों को जीने देने का संदेश दिया है। वे चाहते हैं कि इंसान अपने जीवन में दूसरों के साथ प्रेम और सुख बाँटे। कवि ने इस बात पर जोर दिया है कि सच्चा सुख वही है, जो सबके साथ साझा किया जाए।
प्रसंग:
कवि यहाँ पर परोपकार और प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। वे इस बात का प्रचार करते हैं कि इंसान को न सिर्फ अपने लिए, बल्कि समूचे संसार के लिए जीना चाहिए। उनका उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, और सहिष्णुता का भाव रखें और अपने हर कार्य में समाज का भला सोचें।
व्याख्या:
कवि कहते हैं कि उनका उद्देश्य लोगों को इस बात का पाठ पढ़ाना है कि वे खुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। वे सलाह देते हैं कि जितना अधिक संभव हो सके, हम अपने प्यार को दूसरों में बाँटें। उनकी इच्छा है कि हमारी मुस्कान इतनी सच्ची और प्यारी हो कि धूल में लिपटे, दबे-कुचले लोग भी हमारे साथ हँस सकें।
हमें इस तरह चलना चाहिए कि हमारे पैरों से कोई काँटा न कुचला जाए, यानी किसी को तकलीफ न पहुँचे। कवि के अनुसार, हमारा सुख केवल हमारा नहीं होना चाहिए, उसमें पूरे जग का हिस्सा होना चाहिए। जिस प्रकार फूल डाल को सुंदर बनाने से पहले पूरे बगीचे की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार हमारा सुख भी सभी के लिए होना चाहिए।
इन पंक्तियों में कवि एक महान मानवीय संदेश देते हैं कि हमें प्रेम, सहयोग और सहानुभूति से जीवन जीना चाहिए। उनके लिए हर व्यक्ति अपना है, और वे समूचे संसार को अपना घर मानते हैं।
कोई नहीं पराया कविता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न :
(1) कवि गोपाल दास ‘नीरज’ किसे अपना घर मानते हैं?
उत्तर :-सारे संसार को
(2) कवि ‘नीरज’ का आराध्य कौन है?
उत्तर :-आदमी
(3) ‘कोई नहीं पराया’ में कवि क्या सिखलाना चाहते हैं-
उत्तर :-जियो और जीने दो की भावना
(4) इस कविता का मुख्य संदेश है –
उत्तर :-सारा संसार अपना घर है
कोई नहीं पराया कविता का लघुत्तरीय प्रश्न :
(1) कवि मंदिर मस्जिद के बजाय कहाँ सिर टेकना चाहता है?
उत्तर :-कवि मंदिर-मस्जिद के बजाय हर इंसान के भीतर स्थित देवालय में सिर टेकना चाहता है। वह मानता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।
(2) कवि को किस पर अभिमान है और उसे क्या भाता है?
उत्तर :-कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है, और उसे मनुष्यत्व अधिक प्रिय है, देवत्व की कल्पना या अमरत्व की प्राप्ति से भी अधिक।
(3) कवि को स्वर्गसुख की कहानियों से ज्यादा क्या प्रिय है?
उत्तर :-कवि को स्वर्गसुख की कहानियों से ज्यादा अपनी धरती प्यारी है। उसे अपनी धरती सौ-सौ स्वर्गों से भी अधिक सुकुमार और सुंदर लगती है।
(4) कवि किस प्रकार हँसने और चलने का संदेश देता है?
उतर :-कवि इस तरह हँसने का संदेश देता है कि हमारी हँसी से दलित और पीड़ित लोग भी मुस्कुरा सकें। चलने के लिए वह इस प्रकार चलने का संदेश देता है कि हमारे कदमों से कोई काँटा कुचला न जाए, अर्थात किसी को भी हमारी वजह से तकलीफ न हो।
कोई नहीं पराया कविता का बोधमूलक प्रश्न : :
(1) इस कविता को पढ़कर क्या आपको लगता है कि आज भी एकता विद्यमान है?
उत्तर :- इस कविता को पढ़कर यह एहसास होता है कि कवि ने संपूर्ण मानवता में एकता की भावना का संदेश दिया है। हालाँकि, आज के समय में एकता को कई स्थानों पर संकीर्ण विचारों और मतभेदों ने चुनौती दी है, फिर भी कवि के विचार यह प्रेरणा देते हैं कि यदि हम सभी मिलकर प्रेम और मानवता को अपनाएँ, तो एकता को पुनः स्थापित किया जा सकता है।
(2) 'मुझको अपनी मानवता पर बहुत-बहुत अभिमान है' का भाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर :-“मुझको अपनी मानवता पर बहुत-बहुत अभिमान है” का भाव यह है कि कवि को मनुष्य होने पर गर्व है। उसे मानवता के मूल्य, जैसे प्रेम, करुणा, और सहानुभूति, अत्यधिक प्रिय हैं। कवि का मानना है कि सच्चा धर्म मानवता का पालन करना और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना है। इसलिए, उसे अपने मानवीय गुणों पर गर्व है।
(3) 'हँसो इस तरह, हँसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी' का क्या तात्पर्य है?
उत्तर :-“हँसो इस तरह, हँसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी” का तात्पर्य यह है कि हमारी मुस्कान और खुशियों में इतनी सच्चाई और उदारता होनी चाहिए कि समाज में जो गरीब, असहाय, और दलित वर्ग है, वे भी हमारे साथ हँस सकें और हमारे सुख का हिस्सा बन सकें। यह पंक्ति समता और करुणा की भावना को बढ़ावा देती है।
(4) कवि प्यार को बाँटने की सलाह क्यों देता है?
उत्तर :-कवि प्यार को बाँटने की सलाह इसलिए देता है क्योंकि वह मानता है कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को एक-दूसरे के करीब ला सकती है। जब हम अपने प्यार को दूसरों में बाँटते हैं, तो नफरत और भेदभाव कम होते हैं और समाज में एकता, शांति, और खुशहाली बढ़ती है।